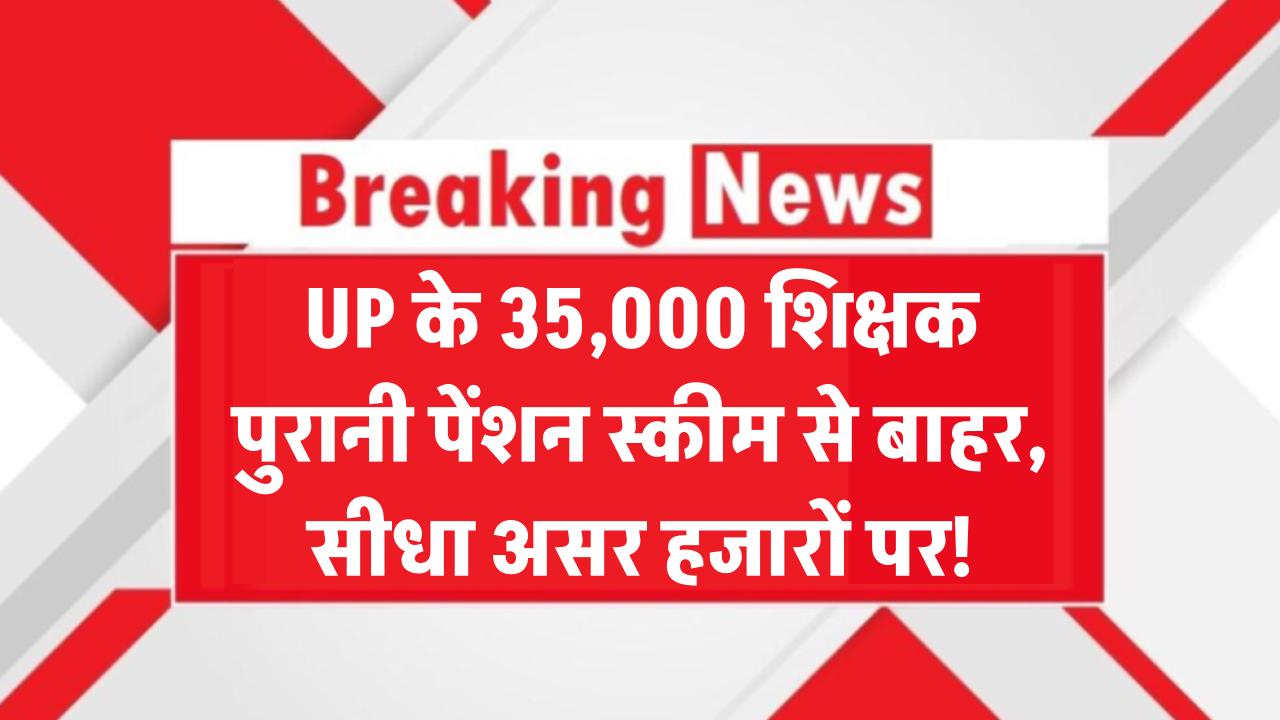इस्लाम धर्म में जब सभी बराबरी के सिद्धांत पर आधारित हैं, और पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि न कोई जाति है, न ऊंच-नीच, तो फिर मुसलमानों में जाति प्रथा कैसे और क्यों दिखाई देती है? यह सवाल आज के समय में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है, जब देश में जातिगत जनगणना की तैयारी हो रही है और हर धर्म की जातियों की गिनती की जाएगी।
इस्लाम का मूल सिद्धांत: सब इंसान बराबर
पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने अंतिम भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि “किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई श्रेष्ठता नहीं है। न किसी गोरे को काले पर और न किसी काले को गोरे पर, सिवाय तकवे (परहेजगारी) के।” यह इस्लाम के बराबरी के उस सिद्धांत को दर्शाता है जहां जन्म, नस्ल, या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता।
शायर अल्लामा इकबाल के शब्दों में भी यह विचार झलकता है: “एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद-ओ-अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज़।” यह संदेश देता है कि नमाज के दौरान अमीर-गरीब, मालिक-गुलाम सब एक समान हैं।
भारतीय मुसलमानों में जाति कैसे आई?
हालांकि इस्लाम के इन आदर्शों के बावजूद भारतीय मुसलमानों में जाति व्यवस्था एक हकीकत बन चुकी है। इसका प्रमुख कारण भारतीय सामाजिक ढांचे की गहरी पैठ है। जब इस्लाम भारत में आया, तब लाखों लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, लेकिन उनके सामाजिक ढांचे यानी जाति में परिवर्तन नहीं हुआ।
ऋग्वेद और मनुस्मृति में वर्णित जाति व्यवस्था के प्रभाव ने भारतीय इस्लाम को भी प्रभावित किया। प्रारंभ में कर्म आधारित जाति व्यवस्था थी, जो बाद में जन्म आधारित हो गई। उसी पैटर्न पर मुसलमानों में भी जातियां विकसित हुईं।
भारतीय मुस्लिम समाज में जाति की परतें
भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों को तीन मुख्य वर्गों में बांटा गया है: अशराफ, अजलाफ, और अरजाल।
अशराफ वे माने जाते हैं जो अरब, तुर्क, अफगान या ईरानी मूल के माने जाते हैं — जैसे सैय्यद, शेख, पठान और मुगल।
अजलाफ वे जातियां हैं जो पेशेवर या शिल्प आधारित समुदाय से आती हैं — जैसे अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, दर्जी, तेली।
अरजाल वे समुदाय हैं जिन्हें सामाजिक रूप से सबसे निचला स्थान मिला — जैसे मेहतर, हलालखोर, मोची, नट, भंगी।
इस वर्गीकरण के पीछे धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक कारण रहे हैं। मौलाना शफी उस्मानी और मौलाना अशरफ अली थानवी जैसे धार्मिक विद्वानों ने भी जातियों का उल्लेख करते हुए कुछ समुदायों को ‘कमतर’ बताया।
मसूद आलम फलाही की किताब भारत में जाति और मुसलमान में यह बात विस्तार से कही गई है कि कैसे मुस्लिम समाज की जाति संरचना हिंदू वर्ण व्यवस्था की तरह काम करती है।
व्यवहार में भी मौजूद है जातिगत भेदभाव
हालांकि धर्म के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं दिखता, लेकिन सामाजिक व्यवहार में भेदभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
उदाहरण के तौर पर, सैय्यद परिवारों में अपनी ही जाति में शादी करने की परंपरा है। शादी, रोजगार, समाज में स्थान, यहां तक कि कब्रिस्तान भी जातियों के अनुसार अलग-अलग देखे जा सकते हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे संभल में यह बात स्पष्ट देखी जा सकती है, जहां तुर्क और लोधी मुसलमानों के बीच अलग-अलग मोहल्ले और सामाजिक तनाव हैं।
जातिगत जनगणना में सामने आएगा सच
भारत सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा से अब मुसलमानों की जातियों की सही तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। इससे यह पता चल सकेगा कि कौन-कौन सी मुस्लिम जातियां सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कितनी पिछड़ी हैं। आज की तारीख में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम जातियां ओबीसी (Other Backward Classes) में आती हैं, लेकिन वे आरक्षण और अन्य सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ नहीं उठा पातीं क्योंकि उनकी पहचान अस्पष्ट रही है।
इस्लामी आदर्श और भारतीय हकीकत के बीच टकराव
इस्लामिक आइडियलिज़्म और भारतीय सामाजिक वास्तविकता के बीच यह टकराव ही जाति व्यवस्था के रूप में सामने आता है। धर्म भले ही सबको बराबर माने, लेकिन सामाजिक ढांचा इसे स्वीकार नहीं कर पाया। यही कारण है कि इस्लाम के समतावादी सिद्धांत के बावजूद भारतीय मुसलमान भी जाति व्यवस्था से अछूते नहीं रह सके।
अब जब सरकार इस विषय पर आंकड़े इकट्ठा करने जा रही है, तो यह बहस फिर से ज़ोर पकड़ रही है कि क्या मुसलमानों को भी जाति आधारित आरक्षण मिलना चाहिए, और क्या वे भी हिंदू समाज की तरह जाति की जकड़न में फंसे हैं?